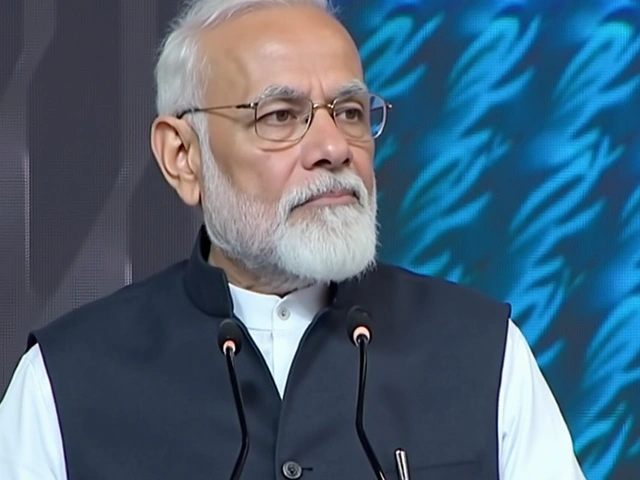एक सोशल मीडिया पोस्ट, दो दिन का वक्त और सियासत में भूचाल—लोकनीति-CSDS के सह-निदेशक संजय कुमार की X (ट्विटर) पोस्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति में यही किया। 17 अगस्त 2025 को उन्होंने 2024 के लोकसभा और 2024 विधानसभा चुनावों के बीच कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में "असामान्य उछाल-गिरावट" का दावा किया। पोस्ट में कहा गया कि नासिक वेस्ट में करीब 47.38% और हिंगणा में 43.08% पंजीकृत मतदाता बढ़े, जबकि रामटेक और देवळाली में लगभग 40% की गिरावट आई। आंकड़े दिखते ही कांग्रेस नेताओं—खासकर राहुल गांधी—ने इन्हें 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उद्धृत करना शुरू कर दिया।
टाइमिंग ने कहानी को और तगड़ा बनाया। उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'वोट हेराफेरी' के आरोपों को खारिज किया था, हालांकि किसी नेता का नाम नहीं लिया। ऐसे में संजय कुमार की पोस्ट विपक्ष के लिए हथियार जैसी दिखी—और सत्ता पक्ष के लिए निशाना। पोस्ट 40 घंटे तक X पर बनी रही और 34 हजार से ज्यादा बार देखी गई।
दो दिन बाद सुर बदला। 19 अगस्त को संजय कुमार ने सार्वजनिक माफी मांगते हुए पोस्ट डिलीट कर दी। उनका शब्दश: बयान था—"I sincerely apologise for the tweets posted regarding Maharashtra elections. Error occurred while comparing data of 2024 LS and 2024 AS. The data in row was misread by our Data team. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing any form of misinformation." यानी तुलना के दौरान रो डेटा पढ़ने में टीम से गलती हो गई और गलत पोस्ट हो गई।
इसके बाद BJP ने इस गलती को महज़ तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि 'कन्फर्मेशन बायस' का नतीजा बताया। पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़ों का प्रचार किया और CSDS को 'झूठ की फैक्ट्री' तक कहा। दूसरी ओर, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे BJP की बौखलाहट बताया और दोहराया कि 'वोट चोरी' के आरोप सिर्फ एक पोस्ट पर आधारित नहीं हैं।
मामला यहीं नहीं रुका। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)—जो CSDS को वित्त पोषण करती है—ने संस्थान को कारण बताओ नोटिस भेज दिया, यानी डेटा की गड़बड़ी और प्रक्रियात्मक चूक पर औपचारिक जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने भी संजय कुमार की माफी का संज्ञान लिया और कहा कि कई विपक्षी नेताओं ने उन्हीं के आंकड़ों को आधार बनाकर आयोग पर सवाल उठाए थे।
यह विवाद दो बड़े सवालों की तरफ इशारा करता है—पहला, चुनावी डेटा जैसे संवेदनशील विषय पर शोध संस्थान किस प्रक्रिया से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं; दूसरा, राजनीतिक बयानबाज़ी में सोशल मीडिया के 'फर्स्ट इम्प्रेशन' का वजन कितना होता है। संजय कुमार की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि स्रोत डेटा/शीट स्तर पर पंक्ति-पढ़ने (रो-रीडिंग) की गलती हुई। लेकिन जब इसी गलती को बड़े दावों की भाषा में पेश किया जाता है तो इसका असर सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहता—यह सार्वजनिक भरोसे को हिलाता है।
आम तौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में बदलाव होना असामान्य नहीं है—नई उम्र के मतदाता जुड़ते हैं, मृत्यु/डुप्लीकेट हटते हैं, स्थानांतरण और सुधार होते हैं। लेकिन 40–47% जैसे भारी उतार-चढ़ाव संकेत देते हैं कि या तो डेटा की यूनिट/सीमा गलत ली गई (जैसे किसी सेक्शन/वार्ड को संपूर्ण मतदाता सूची समझ लेना), या फिर अलग-अलग समय की सूची/रोल के संस्करणों की तुलना में तकनीकी त्रुटि हुई। जिस तरह संजय कुमार ने 'रो मिसरीड' कहा, वह बताता है कि शीट में कॉलम/पंक्ति की असंगत मैपिंग से निष्कर्ष उलट गए।
सवाल यह भी है कि ऐसी पोस्ट बाहर जाने से पहले शोध संस्थान के भीतर कौन-कौन सी फिल्टरिंग होती है। मजबूत प्रक्रिया में आम तौर पर ये कदम शामिल होते हैं—कच्चे डेटा का दोहरी जांच, कोड/कैल्कुलेशन की पीयर-रिव्यू, मेटाडेटा का स्पष्ट ब्योरा (डेटा किस तारीख का है, यूनिट क्या है, सीमाएं क्या हैं), और सार्वजनिक रिलीज से पहले "सेंस-चेक"—यानी परिणाम सामान्य अनुभव/भौतिक वास्तविकता से मेल खाते हैं या नहीं। अगर किसी सीट पर मतदाता एक साल में आधे के आसपास घट-बढ़ रहे हों, तो यह 'रेड फ्लैग' होता जिसे रोककर दुबारा जाँचना चाहिए था।
राजनीतिक स्तर पर विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने के मौके की तरह देखा। सत्ता पक्ष ने पलट कर कहा कि यह एक तैयार नैरेटिव का हिस्सा है—पहले आरोप तय, बाद में आंकड़े ढूंढ़ो। सच बीच में कहीं है—डेटा की गलती हुई, स्वीकार भी हुई; लेकिन इससे चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर फैला अविश्वास भी दिखा जो सोशल मीडिया पर मिनटों में कई गुना बढ़ जाता है।
ICSSR का शो-कॉज़ नोटिस संस्थागत जवाबदेही की तरफ कदम है। इसमें आम तौर पर तीन चीजें माँगी जाती हैं—गलती कैसे हुई, सुधारात्मक कदम क्या होंगे, और भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए SOP क्या होगा। अगर जवाब संतोषजनक न हो, तो फंडिंग की समीक्षा, आंतरिक ऑडिट या बाहरी समीक्षा जैसे कदम उठ सकते हैं। शोध जगत के लिए यह चेतावनी है कि सार्वजनिक संवाद में आने वाला हर आंकड़ा सिर्फ अकादमिक नहीं, राजनीतिक असर भी पैदा करता है।
चुनाव आयोग के लिए यह प्रकरण दोहरी चुनौती है—पहली, गलत दावों का त्वरित प्रतिवाद; दूसरी, पारदर्शिता बढ़ाकर भरोसा मजबूत करना। आयोग ने बीते वर्षों में वोटर हेल्पलाइन, मतदाता सूची के ऑनलाइन अपडेशन और SSR (समरी रिवीजन) जैसी प्रक्रियाएँ डिजिटल की हैं। लेकिन जब हाई-वॉल्यूम गलत सूचना तेज़ी से फैलती है, तो रियल-टाइम डेटा स्पष्टीकरण, सार्वजनिक डैशबोर्ड और समय-समय पर तकनीकी ब्रीफिंग जैसे टूल और आक्रामक होने चाहिए।
मीडिया और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी कम नहीं। किसी भी सनसनीखेज आंकड़े को तत्काल बयानबाज़ी में बदलने से पहले तीन सरल चेक काम आते हैं—मूल स्रोत और डेटा-डिक्शनरी देखें, वैकल्पिक आधिकारिक स्रोत से क्रॉस-वेरिफ़ाई करें, और विशेषज्ञ से 'प्लॉजिबिलिटी चेक' कराएँ। यह एक घंटे की देरी, कई दिनों के विवाद बचा सकती है।
सोशल मीडिया की पारिस्थितिकी इस आग को हवा देती है। एल्गोरिद्म नई/चौंकाने वाली बात को आगे धकेलते हैं; रीट्वीट/फॉरवर्ड की गति किसी भी स्पष्टीकरण से तेज होती है। ऐसे में जिन खातों का असर अधिक है—शोधकर्ता, पत्रकार, नेता—उनके लिए "ड्राफ्ट-टू-पब्लिश" के बीच 'कूलिंग-ऑफ' रूल, यानी 30–60 मिनट का रिव्यू गैप, एक व्यावहारिक उपाय हो सकता है।
CSDS और लोकनीति का नाम चुनावी अध्ययन में वर्षों से जुड़ा रहा है। इसलिए इस एक घटना का असर संस्थागत साख पर पड़ेगा ही। पारदर्शी सुधार—जैसे रॉ डेटा/कोड का ओपन-रिलीज, थर्ड-पार्टी मेथडोलॉजी ऑडिट, और स्पष्ट एराटा—विश्वास बहाल करने के सीधे रास्ते हैं। संजय कुमार की सार्वजनिक माफी एक शुरुआती कदम है; असली परीक्षा यह होगी कि आगे डेटा गवर्नेंस कैसे कसी जाती है।
जहाँ तक राजनीति की बात है, 'वोट चोरी' जैसे बड़े आरोप तभी टिकते हैं जब प्रमाण सुसंगत, व्यापक और स्वतंत्र रूप से सत्यापित हों। अलग-अलग सीटों पर असामान्य पैटर्न दिखे तो उनका फॉरेंसिक—बूथ-लेवल पर रोल वेरियन्ट, नेट-एडिशन/डिलीशन, माइग्रेशन—से करना पड़ता है। एक वायरल शीट या थ्रेड किसी भी पक्ष के लिए ठोस सबूत नहीं बन पाती।
यह पूरा प्रकरण याद दिलाता है—डेटा शक्ति है, पर बिना संदर्भ के जोखिम भी। एक पंक्ति की चूक सिर्फ स्प्रेडशीट नहीं बिगाड़ती, लोकतांत्रिक विमर्श को भी झटका देती है। अगला कदम सभी के लिए साफ है—कम शोर, ज्यादा जांच; कम अनुमान, ज्यादा प्रमाण।
यह मामला सिर्फ एक ट्वीट की गलती नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भरोसे की जड़ में दरार है।
जब कोई मान्यता प्राप्त संस्था अपनी डेटा को बना-भुना कहती है, तो जनता की जागरूकता खतरे में पड़ती है।
नासिक वेस्ट और हिंगाणा में सार्वजनिक रूप से दिये गये 40‑50% के बदलाव को देख कर हर नागरिक को हकलाना पड़ता है।
ऐसे आंकड़े बिना गहरी जांच के सोशल मीडिया पर छा जाते हैं और सियासत में आग लगा देते हैं।
CSDS की नजर में यह “रो‑रीडिंग” एक मामूली त्रुटि लगती है, पर असली असर वोटर एंगेजमेंट पर पड़ता है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी यह पोस्ट तुरंत तालिका बन गया।
इससे न केवल कांग्रेस के नेताओं को प्रयोगात्मक सामग्री मिली, बल्कि भाजपा को प्रतिशोध का अवसर भी मिला।
इस त्रुटि ने दोनों पक्षों को एक फर्जी युद्ध में फँसा दिया, जहाँ हर तरफ से आरोप‑प्रत्यारोप होते रहे।
डेटा वैज्ञानिकों को अब अपनी प्रोटोकॉल को दोबारा जांचना चाहिए, जैसे कि ड्यूल‑कंट्रोल और पियर‑रिव्यू।
अगर ऐसी चूक दोहराई गई तो संस्थान को फंडिंग का खतरा भी झेलना पड़ सकता है।
जनता को भी चाहिए कि वह आँकड़ों को तुरंत साक्ष्य के रूप में न ले, बल्कि पुष्टि के बाद ही भरोसा करे।
सोशल मीडिया की गति इतनी तेज़ है कि एक छोटी सी गलती भी रातोंरात वायरल हो जाती है।
इस परिदृश्य में “कूलिंग‑ऑफ” रूल लागू करना आवश्यक है, ताकि हर पोस्ट को पुनः जाँचने का समय मिल सके।
मेरे विचार में, बोर्डों को ओपन‑डेटा प्लेटफ़ॉर्म खोलना चाहिए, जहाँ कोई भी विशेषज्ञ कोड देख सके।
तब ही हम इस तरह की “वोट चोरी” की अफ़वाहों को ठोस साक्ष्य के बिना खारिज कर पाएँगे।
अंत में, हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र की शक्ति डेटा में नहीं, बल्कि उस डेटा के सही उपयोग में है।
डेटा की गलती समझ आई लेकिन टीम के प्रयास को भी सराहना चाहिए
भविष्य में ऐसी रोकथाम के कदम जरूरी हैं
ऐसे बड़े दावे अक्सर आँकड़ों के सतही विश्लेषण से उभरते हैं
वास्तविकता में कई बार जटिल जनसांख्यिकीय व्यवधान होते हैं
इसे तुरंत “वोट चोरी” कहना नजाकत नहीं है
साथियों, यह सत्य है कि डेटा जटिल हो सकता है परन्तु वैज्ञानिक विधियां इसे स्पष्ट कर सकती हैं; उचित समीक्षा प्रक्रिया से भविष्य में ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं होगी; आशा है कि सभी पक्ष मिलकर सटीकता को प्राथमिकता देंगे
वाह भई ये डेटा की गलती तो पूरे शहर को हिला गयी है
कौन सोचता था कि एक छोटी सी रो‑रीडिंग इतना बड़ा नाटा पैदा कर देगा
अब सभी को सोचना पड़ेगा कि किस पर भरोसा करना है
हँ, तुम सही कह रहे हो
ऐसी चूक से सबको सीख लेनी चाहिए
आगे से दोबारा चूक न हो
इनथा एरर को ट्रीट करने के लिये हमे स्टैटिस्टिकल वैरिएन्स एनालिसिस और कॉन्फिडेंस इंटर्वल री-कैलकुलेशन लागू करना पड़ेगा; मौजूदा डेटासेट में सैंपल बायस तथा सिलेक्टिव बायस की संभावनाएं उच्च हैं, इसलिए रिग्रेशन मॉडेल री-फ़िट करना अनिवार्य होगा
भाइयों डेटा चेक करने में थोडी गलती हो गयी थी पर बहुत बुरी बात ना है
अगली बार हम सब मिलके दोबारा वैरिफ़ाइ कर लेंगे इते
मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रकार की सार्वजनिक गलतफ़हमी कितना तनाव पैदा करती है।
जब राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का मुद्दा उठता है तो हर नागरिक की नींदें उड़ जाती हैं।
संवेदनशील डेटा को जल्दी-जल्दी शेयर करना जोखिम भरा होता है, यह हमें पिछले कई घटनाओं से पता चलता है।
साथ ही, राजनीतिक दलों द्वारा तुरंत इस डेटा को अपने एजेंडा में इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ऐसी स्थितियों में मीडिया को भी जिम्मेदारी से तथ्यों को जांचना चाहिए, न कि सनसनी के पीछे भागना।
डाटा टीम की गलती को स्वीकार कर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, यह एक सकारात्मक कदम है।
लेकिन इसे केवल “माफ़ी” तक सीमित नहीं रखना चाहिए; सुधारात्मक उपायों को भी लागू करना जरूरी है।
आगे से डेटा की दोहरी जाँच, पीयर‑रिव्यू और सार्वजनिक ओपन‑डेटा प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया जाना चाहिए।
नागरिकों को भी आलोचनात्मक सोच अपनानी चाहिए, हर समाचार को बिना पूछे नहीं मानना चाहिए।
अंत में, हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र की शक्ति डेटा में नहीं, बल्कि उस डेटा के सही उपयोग में निहित है।
आशा करता हूँ कि इस घटना से सभी संस्थानों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नई लहर आएगी।
और सबसे महत्वपूर्ण, जनता को इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए।
अभी के लिए चलिए इस गलती को सीख कर भविष्य में अधिक सावधानी बरतते हैं।
ग्लेडिएटेड विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि डेटा त्रुटि ने न केवल सार्वजनिक विमर्श को विकृत किया बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता को भी हटा दिया; इस प्रकार के मामलों में उच्चस्तरीय प्रोटोकॉल का अभाव अनिच्छित परिणामों को जन्म देता है; इसलिए, कड़े मानक स्थापित करना अनिवार्य है
विचारधारा चाहे जो भी हो, तथ्यों की पारदर्शिता और डेटा की अखंडता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए; नीतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सम्मिलित करके ही हम ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं; इस दिशा में सामुदायिक सहभागिता और स्वतंत्र ऑडिट आवश्यक हैं
यह अत्यंत स्पष्ट है कि इस प्रकार की लापरवाही राष्ट्रीय अखंडता पर धुंधला धब्बा बनकर उभरती है; हमे ऐसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए; राष्ट्र की गरिमा को बचाने हेतु कठोर जवाबदेही और कड़ी सजा अनिवार्य है; ऐसे त्रुटियां केवल अकादमिक गलती नहीं, बल्कि देश के भविष्य के प्रति दुष्कर्म हैं; अब समय आ गया है कि सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें; अन्यथा विश्वसनीयता का पतन अपरिहार्य है
ऐसा बकवास अब हाईलाइट नहीं होना चाहिए!
इस डेटा एरर को कर्तव्य की ओर सिमित करि जाऐ तो ही संस्थान की विश्वसनीयता पुनः स्थापित हो सकेगी; सही प्रोसेस की अंपीदांस न होने पर फिर ऐसा सावाला प्रकटीकरण फिर न हो, यह आवश्यक है
भाई साब, ये सब फालतू का ड्रामा है, असली चीज़ तो ये है कि हर बार जब कोई बड़ा डेटा वाला आदमी बोलता है तो सबको उलझा देता है, बस समझ लो, ऊपर से वोटर लिस्ट बदलना रोज़मर्रा की बात है, पर नेट पे बड़े-बड़े नाटक होते हैं
वास्तव में, जब हम इस तरह के संवेदनशील डेटा को देखते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को कई आयामों से परखें; अर्थात्, न केवल आँकड़ों की सतही जाँच करनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे के कारणों, संभावित त्रुटियों व डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को भी समझें; यह सब तभी संभव है जब संस्थान अपने सर्वेक्षण प्रोटोकॉल को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए, तथा डेटा के प्रत्येक चरण की लेखा‑जोखा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे; ऐसा करने से न केवल शून्य‑त्रुटि के निकट पहुँचेंगे, बल्कि जनता का भरोसा भी फिर से जीतेंगे; इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ओपन‑डेटा फ्रेमवर्क को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे स्वतंत्र शोधकर्ता भी डेटा की वैधता की पुष्टि कर सकें; अंततः, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण तब संभव होगा जब सभी हितधारक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को अपनाएँ, और प्रत्येक पक्ष को डेटा‑पर‑आधारित निर्णय लेने का अवसर मिले; अतः, इस घटना को सीख के रूप में ले कर भविष्य में ऐसे जोखिमों को न्यूनतम करने का संकल्प लें
ओह, क्या बात है! एक Excel की सिलिकॉन गलती से पूरी राजनीति का मुँह बदल गया, वाह कितना रोमांचक!